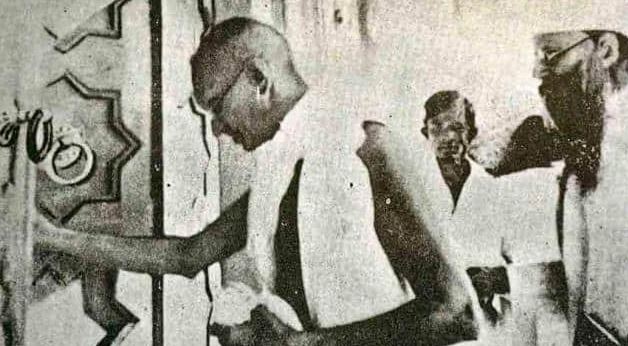
जब महात्मा गांधी को काशी के पण्डा ने गालियाँ सुनाकर अपमानित किया। काशी तीर्थ यात्रा महात्मा की जुबानी।
शिव कुमार शुक्ला
“अब तीसरे दर्जे की यात्रा की चर्चा यहीं छोड़ कर काशी के अनुभव सुनिए। सुबह मैं काशी उतरा। मैं किसी पण्डे के यहां उतरना चाहता था। कई ब्राह्मणों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उनमें से जो मुझे साफ-सुथरा दिखाई दिया, उसके घर जाना मैंने पसन्द किया। मेरी पसन्दगी ठीक निकली। ब्राह्मण के आंगन में गाय बधी थी। घर दुमंजिला था। ऊपर मुझे ठहराया। मैं यथा विधि गंगा स्नान करना चाहता था। और तब तक निराहार रहना था । पण्डे ने सारी तैयारी कर दी। मैंने पहले से कह रक्खा था कि सवा रुपए से अधिक दक्षिणा मैं नहीं दे सकूगा , इसलिए उसी योग्य तैयारी करना। पण्डे ने बिना किसी झगड़े के मेरी बात मान ली। कहा- “हम तो क्या गरीब और क्या अमीर, सबसे एक ही सी पूजा करवाते हैं। यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार जो दक्षिणा दे दे वही सही।” मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पण्डे ने पूजा में कोई कोर-कसर रखी हो। बारह बजे तक पूजा-स्नान से निवृत्त होकर मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया। पर वहाँ जो कुछ देखा उससे मन में बड़ा दु:ख हुआ।”
काशी विश्वनाथ मंदिर
” सन् 1891 ई० में जब मैं बम्बई में वकालत करता था, एक दिन प्रार्थना समाज मन्दिर में काशी यात्रा पर एक व्याख्यान सुना था। इसलिए कुछ निराशा के लिए तो वहीं से तैयार हो गया था, पर प्रत्यक्ष देखने पर जो निराशा हुई वह तो धारणा से अधिक थी। संकरी- फिसलनी गली से हारकर जाना पड़ता था शान्ति का कहीं नाम नहीं। मक्खियाँ चारों ओर भिनभिना रही थी। यात्रियों और दुकानदारों का हो-हल्ला असाह्म मालूम हुआ।
“जिस जगह मनुष्य ध्यान एवं भगवच्चिन्तन की आशा रखता हो, वहां उनका नामोनिशान नहीं, ध्यान करना हो तो वह अपने अन्तर में कर ले | हा, ऐसी भावुक बहनें मैंने जरूर देखीं, जो ऐसी ध्यान-मग्न थी कि उन्हें अपने आस पास का कुछ भी हाल मालूम न होता था। पर इसका श्रेय मन्दिर के संचालकों को नहीं मिल सकता। संचालकों का कर्तव्य तो यह था कि काशी विश्वनाथ के आस-पास शान्त, निर्मल, सुगन्धित, स्वच्छ वातावरण-क्या बाह्य और क्या अन्तरिक– उत्पन्न करें, और उसे बनाये रखे| पर इसकी जगह मैंने देखा कि वहाँ नये-से-नये तर्ज की मिठाई और खिलौनों की दुकानें लगी हुई थी।
“मन्दिर पर पहुँचते ही मैंने देखा कि दरवाज़े के सामने सड़े हुए फूल पड़े थे और उनमें से दुर्गन्ध निकल रही थी। अन्दर बढ़िया संगमरमरी फर्श था। उस पर किसी अन्ध-श्रद्धालु ने रुपए जड़ रखे थे; रुपयों में मैल-कचरा घुसा रहता था।
“मैं ज्ञानवापी के पास गया। यहां मैंने ईश्वर की खोज की। वह होगा; पर मुझे न मिला। इससे मै मन-ही-मन घुट रहा था। ज्ञानवापी के पास भी गन्दगी देखी। भेंट रखने की मेरी जरा भी इच्छा न हुई, इसलिए मैंने तो सचमुच ही एक पाई वहाँ चढ़ाई। इस पर पण्डा जी उखड़ पड़े। उन्होंने पाई उठाकर फेंक दी और दो-चार गालियां सुनाकर बोले— “तू इस तरह अपमान करेगा तो नरक में पड़ेगा।”
“चुप रहा। मैने कहा- “महाराज। मेरा तो जो होना होगा वह होगा, पर आपके मुंह से हलकी बात शोभा नहीं देती। यह पाई लेना हो तो ले वर्ना इसे भी गँवायेंगे।” “जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए” कह कर उन्होंने ज्यादा भला-बुरा कहा। मै पाई लेकर चलता हुआ। मैंने सोचा कि महाराज ने पाई गंवाई और मैंने बचा ली। पर महाराज पाई खोने वाले न थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और कहा – “अच्छा रख दे मै तेरे जैसा नहीं होना चाहता। मैं न लूं तो तेरा बुरा होगा।”
“मैंने चुपचाप पाई दे दी और एक लम्बी सांस लेकर चलता बना। इसके बाद भी दो-एक बार काशी-विश्वनाथ गया हूँ, पर वह तो तब, जब महात्मा बन चुका था । इसलिए 1902 के अनुभव भला कैसे मिलते ? खुद मेरे ही दर्शन करने वाले मुझे क्या दर्शन करने देते ? महात्मा के दुःख तो मुझ जैसे महात्मा ही जान सकते हैं । किन्तु गन्दगी और हो-हल्ला तो जैसे -के-तैसे ही वहाँ देखे ।
“परमात्मा की दया पर जिसे शंका हो, वह ऐसे तीर्थ क्षेत्रों को देखे। वह महायोगी अपने नाम पर होनेवाले कितने ढोंग, अधर्म और पाखण्ड इत्यादि को सहन करते हैं। उन्होंने तो कह रखा है: —
ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
अर्थात् जैसा करना वैसा भरना । कर्म को कौन मिथ्या कर सकता है ? फिर भगवान् को बीच में पड़ने की क्या जरूरत है ? वह तो अपने कानून बतलाकर अलग हो गया।

























